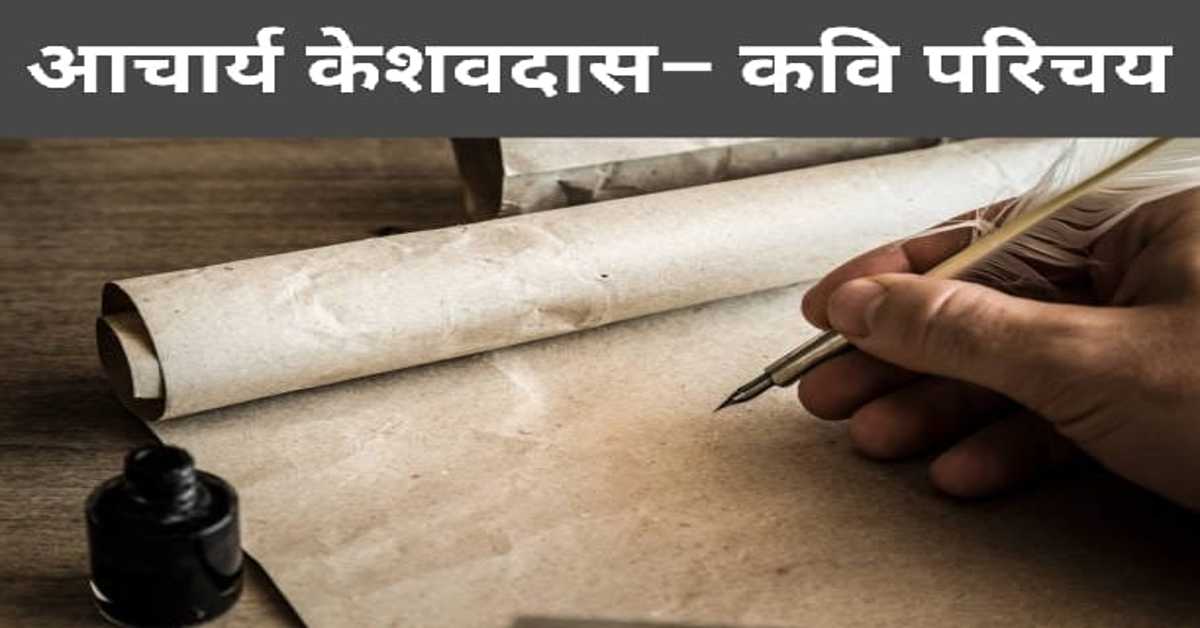
आचार्य केशवदास– कवि परिचय
जीवन-परिचय
आचार्य केशवदास का जन्म सन् 1555 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ओरछा के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम काशीनाथ मित्र था। वे संस्कृत के विद्वान थे। केशवदास को संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। वे तत्कालीन समय के ओरछा नरेश महाराजा रामसिंह के दरबार में कवि थे। उन्हें ज्योतिष, संगीत, वैद्यक, संस्कृति, राजनीति आदि क्षेत्रों में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। केशव स्वभाव से गंभीर एवं स्पष्टवादी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के रीतिकाल की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में स्थापित करने का कार्य किया। इस कार्य हेतु उन्हें हिंदी साहित्य के आकाश में उल्लेखनीय सराहना प्राप्त हुई। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। केशवदास नवीन कवियों के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के जगत को एक नवीन राह दिखायी है। उन्होंने लक्षण ग्रंथ, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य की रचना की है। उन्होंने हिंदी में अलंकार, छंद आदि की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। केशवदास ने की रचनाएँ बहुत जटिल होती हैं। उनकी काव्य रचनाओं का सही अर्थ निकालना एक कठिन कार्य है। अतः इस अनूठी विशेषता के कारण केशवदास को हिंदी जगत के 'कठिन काव्य के प्रेत' के नाम से जाना जाता है। सन् 1617 ईस्वी में केशव इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए।
हिन्दी के इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िए।।
बीती विभावरी जाग री― जयशंकर प्रसाद
महत्वपूर्ण रचनाएँ
केशवदास की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं–
1. रामचंद्रिका
2. रसिकप्रिया
3. कविप्रिया
4. जहाँगीर जस चंद्रिका
5. वीर चरित
6. विज्ञान गीता
7. नख-शिख
8. रसालंकृत मंजरी
हिन्दी के इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िए।।
मैया मैं नाहीं दधि खायो― सूरदास
भावपक्ष
हिंदी जगत में केशव को 'आचार्य' कहकर संबोधित किया जाता है। वे हिंदी के अविस्मरणीय कवि हैं। उन्हें अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। उनकी रचनाओं में अलंकारों का यथोचित प्रयोग किया गया है। उनके अलंकार कौशल के कारण उन्हें चमत्कारवादी कवि माना जाता है। केशव की रचनाओं में प्रयोग किए गए प्रमुख रस श्रृंगार, शान्त, वीर और करूण आदि हैं। उनके काव्य में संयोग और वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन मिलता है। इसके साथ ही पात्रों के संवादों में वीर रस का प्रयोग किया गया है। केशव दरबारी कवि थे। अतः उन्होंने अपने काव्य में विविध नीति निर्देश दिए हैं। वे सदैव ही नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। उनके काव्य में अर्थ का सौंदर्य सराहनीय है। उन्होंने गंभीर एवं गूढ़ अर्थ देने वाले काव्यों की रचनाएँ की हैं।
हिन्दी के इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िए।।
मैया कबहिं बढ़ैगी चोटी― सूरदास
कलापक्ष
केशव ने अपनी रचनाओं में अधिकांशतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार है। उनकी भाषा में विषय, पात्र और संदर्भ में अनुरूप परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कुछ अंशों में भाषा की दूरूहता भी दिखाई देती है। केशवदास ने मुख्य रूप से उपमा, यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का यथोचित प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। इसके अलावा उन्होंने अलंकारिक, व्यंग्यात्मक और संवाद शैली में भी काव्य रचना की है। उनके द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख छंद दोहा, कवित्त, रोला, सवैया, तोरक, छप्पय, त्रिभंगी, दंडक आदि हैं। उन्होंने मात्रिक एवं वर्णिक दोनों छंदों का प्रयोग किया है। केशव के काव्य में संवादों का सौंदर्य अद्वितीय है। काव्य में उनके द्वारा प्रयोग किये गए संक्षिप्त, चुटीले और प्रभावी संवाद उन्हें अन्य कवियों की तुलना में विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।
हिन्दी के इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िए।।
बानी जगरानी की उदारता बखानी जाइ― केशवदास
साहित्य में स्थान
केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य थे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे दरबार के राजकीय ठाट-बाट में रहते थे। इस कारण उनमें पांडित्य प्रवृत्ति की प्रधानता थी। उनके काव्य में वस्तु निरूपण, अलंकार योजना, छंद विधान, शब्द चयन आदि अद्वितीय है। इन्हीं सब अनूठी विशेषताओं के कारण केशवदास हिंदी साहित्य के आकाश में चिरस्मरणीय रहेंगे।
हिन्दी के इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िए।।
बाल्हा मैं बैरागिण हूँगी हो– मीराबाई
आशा है, उपरोक्त जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
धन्यवाद।
R F Temre
rfcompetition.com
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
pragyaab.com




Comments